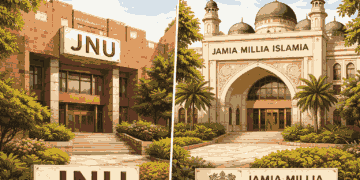“संत दूसरों के बच्चे ही अच्छे लगते हैं…”
माँ की आँखों का सूखापन उनके अक्सर गिरते आँसुओं से ज्यादा चिंताजनक था। बात करते-करते वो कब अपनी यादों के भंवर में फँस गयीं मुझे समझ भी नहीं आया। ऐसा लग रहा था की उनकी आवाज़ मानो किसी पुरानी बावड़ी में गूंजती हुई आ रही थी।
“तू लड़का है न, तू नहीं समझेगा। तुझे नहीं पता बचपन में जब अपने सपनों को अपने हाथों से गला घोंट कर मारना पड़ता है तो कैसा लगता है।”
थोड़ी भूमिका बांधनी पड़ेगी – माँ बचपन में पढ़ाई-लिखाई में रूचि नहीं रखती थीं – उनको तो शौक़ था खेलने का, और वो भी खोखो, कबड्डी, बास्केटबॉल – सब लड़कों के खेल। अब टीकमगढ़ जैसी छोटी-सी जगह, उस पर वक़ील साहब और प्रिंसिपल मैडम की छोटी बेटी – ये सब काम करेगी! बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, ग्वालियर से मामाजी आये मेरी नानी को समझाने कि शादी में अड़चनें होंगी…माँ तो बेपरवाह खेलती रहीं – जब तक अलाहाबाद वाली बड़ी बुआ ने आकर पूरे वाकये पर पूर्णविराम नहीं लगा दिया – “बेटी, झाँसी की रानी झाँसी में ही शोभा देती है, अलाहाबाद में नहीं।”
क्रान्ति – दीवान-ए-आम से लेकर ज़नानाख़ाने तक
बड़ी पते की बात बोली थी बड़ी बुआ जी ने – हम सभी घर के बाहर तो बड़े क्रांतिकारी बनते हैं, लेकिन घर की चारदीवारी में वही जात-धर्म की बातें, वही अंधविश्वास सब एक-एक कर के सामने आते जाते हैं। बड़ों की इज्ज़त करो, अपने हमेशा अपने ही होते हैं, दूसरों के फट्टे टाँग मत अड़ाओ – वो सारी बातें जो हम अपने online अवतार में ठीक उल्टा करते हैं, वही सब अक्सर घर में हम बिना सोचे-समझे सिर झुका कर करते रहते हैं। (गौरतलब है कि ये बातें एक भी खुद में खराब या शोचनीय नहीं हैं। वो जिस भाव से बोली जाती हैं, जिन पूर्वाग्रहों के दलदल में उनका जन्म हुआ है – वह मुझे बहुत दुखी करता है।) कभी माता-पिता का डर, तो कभी वही पुराना, घिसा-पिटा बहाना – “लोग क्या सोचेंगे?”, या आज कल का नया फितूर, “appraisal कहीं खराब न हो जाये…” हम सबको अपने दिल और दिमाग में एक संतुलन तो बनाकर रखना ही पड़ता है, हाँ कि ना? अब भले ही संतुलन बनाना खुद ही एक बहुत ही बुद्धिजीवियों वाला काम क्यों न हो…
मामला अब किताबी न रहा
जब तक बात कुछ दाँव लगाने की नहीं होती तब तक मुंह चलाने में क्या जाता है – मैं online बोल सकता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ, समाजवादी हूँ, साम्यवादी हूँ। लेकिन बात जब शादी की होती है, जब नौकरी की बारी आती है तब तो मैं चुपचाप कामिनी-कांचन को गले लगा लेता हूँ बिना चूँ-चपड़ किये! सारे क्रांतिकारी विचार एक तरफ रह जाते हैं, और मेरे चयन पर नियंत्रण रह जाता है सिर्फ मेरे रूढ़िवादी अचेतन के नेपथ्य में गूंजती कुछ अतीत की बातें, या मीडिया के घिनौने षड्यंत्रों का ताना-बाना जो अँधेरे कमरे में घूमते पतंगे को मकड़ी के जाल जैसा हर तरफ से पकड़ता रहता है – वंश आगे बढ़ाना है, आदर्श दंपति ऐसे ही होने चाहिए, वगैरह-वगैरह।
“जो घर बारे आपना, चले हमारे संग “
हमने एक बहुत महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है – हमने आज कम से कम अपना विरोध जताया है, अपना आक्रोश भले ही कुछ समय के लिए ही सही लेकिन सड़कों पर प्रदर्शित किया है। अब ज़रूरत है हमें यही क्रांति की आग जलाए रखने की और लगातार गहरा आत्मनिरीक्षण करने की: जिन सिद्धांतों को हम online अनजान व्यक्तियों के सामने खुलेआम प्रतिपादित करते रहते हैं, उनको हम अपने निजी जीवन में कितना अमल करते हैं? किस तरह से हम अपने पूर्वाग्रहों को शिद्दत से बनायी हुई अपने सिद्धांतों से जोड़ पायेंगे? ये और ऐसे ही कुछ और सवाल आने वाले समय में निर्धारित करेंगे कि हमने जिस क्रांति को अपने देश में शुरू किया है उसको गाँव-गाँव, गली-गली में कितने आसानी से पचाया जायेगा।
आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है हमारे देश में विद्रोह की जगह घर में नहीं, सिर्फ राजनैतिक मंच पर है? कृपया अपने अनुभव और विचार हमारे साथ बाँटें – आपकी राय जानने का हमें इंतज़ार रहेगा।